Mahabharat PDF Download in Hindi | महाभारत की E Book डाउनलोड करें हिंदी भाषा में
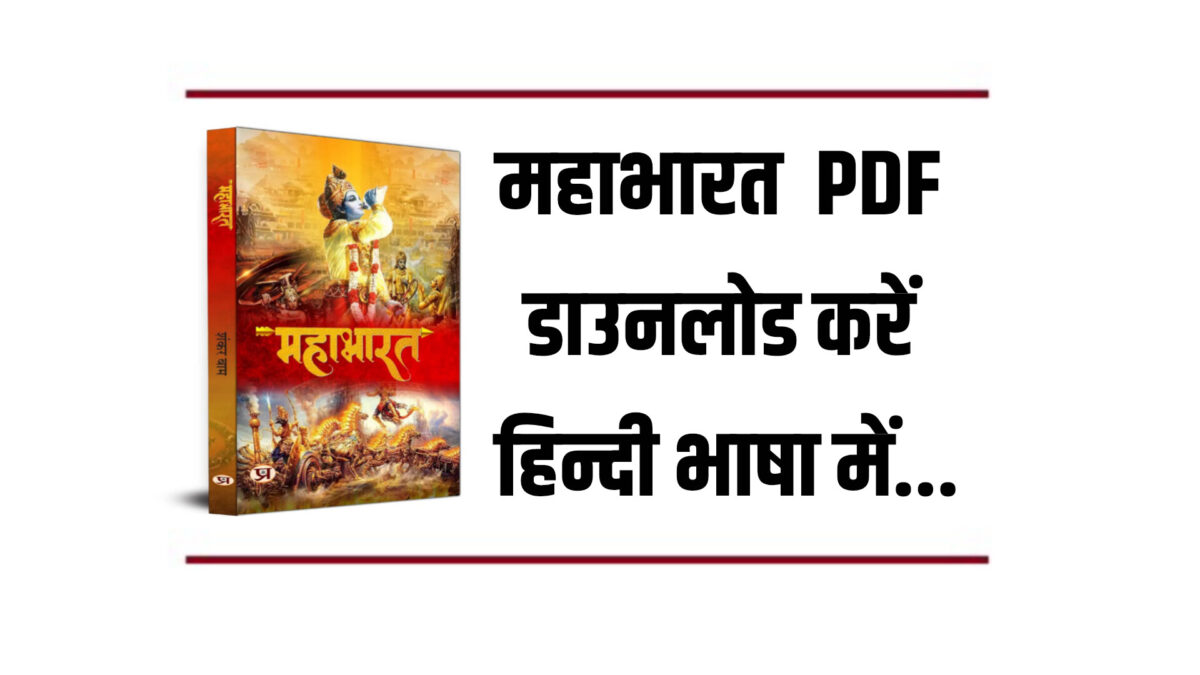
महाभारत पढ़ते हुए लगता है, मानो इंसानी जीवन का हर रंग इसमें समा गया हो कहीं वीरता है, कहीं छल, कहीं करुणा, और कहीं अजीब सी दुविधा. ” धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ” से आरंभ यह कथा सिर्फ़ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मन और समाज का एक बड़ा इम्तहान भी है !
परंपरा वेदव्यास को इसका कृतिकार मानती है, और इसे ” इतिहास ” तथा ” पूर्ण ग्रंथ ” कहा गया है, क्योंकि यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का गंभीर विमर्श मिलता है ! सच कहूँ तो, पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा था, तो लगा कि यह किताब मुझे पढ़ रही है ! सवाल मेरे भीतर उठते थे, बाहर नहीं !
यह महाकाव्य अठारह ( 18 ) पर्वों में विभाजित है ! कुल श्लोक संख्या परंपरा में एक लाख कही जाती है पर यहाँ मतभेद हैं और अलग अलग पाठ परंपराएँ भी हैं ! रचना काल लगभग ईसा पूर्व चार सौ ( 400 ) से ईस्वी चार सौ ( 400 ) के बीच माना जाता है, हालांकि विद्वान इस पर बहस करते रहे हैं ! इस बहस का मतलब साफ है : महाभारत कई पीढ़ियों की स्मृतियों और विमर्शों से बनता संवरता रहा !
कथा का मुख्य मंच कुरु वंश और हस्तिनापुर है लेकिन इसका विस्तार भरतवंश, अनेक जनपदों, तीर्थों और आश्रमों तक जाता है ! भीष्म पर्व में ही भगवद्गीता आती है अध्याय एक ( 1 ) से अठारह ( 18 ) जहाँ अर्जुन और कृष्ण का संवाद जीवन दर्शन की रीढ़ बनकर उभरता है ! स्कूल की सभा में जब पहली बार गीता पाठ सुना, तो लगा यह सवाल अर्जुन से ज़्यादा मेरा ही है : मैं किस कर्तव्य को प्राथमिकता दूँ ?
कथा का केंद्र पांडवों और कौरवों के बीच उत्तराधिकार और सम्मान की लड़ाई है ! पांडु के पांचों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और धृतराष्ट्र के सौ ( 100 ) पुत्रों में अग्रणी दुर्योधन, दोनों ओर महत्वाकांक्षा और परंपरा की टक्कर है ! बचपन से ही ईर्ष्या के बीज बो दिए जाते हैं शस्त्र विद्या में प्रतिस्पर्धा, गुरु शिष्य संबंधों में पक्षपात का आभास, और दुर्योधन कर्ण की दोस्ती !
लाक्षागृह का षड्यंत्र, द्रौपदी स्वयंवर, और फिर द्यूत ये मोड़ पांडवों के विघटन और अपमान की जमीन तैयार करते हैं ! द्रौपदी का अपमान केवल दरबार का अपराध नहीं ; यह हमारी सामूहिक चेतना पर चोट है ! और हाँ, यह चोट बार बार याद आती है ! बार बार ! वनवास और अज्ञातवास में पांडव मित्र राष्ट्र और आत्मविश्वास जुटाते हैं पर शांति की कोशिशें विफल होती हैं ! कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं लौटते हैं तो मन भारी ! अंततः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपरिहार्य हो जाता है !
युद्ध अठारह ( 18 ) दिन चलता है ! रणनीति है, शौर्य है, और छल भी ! भीष्म की शरशय्या, द्रोण का पतन, कर्ण अर्जुन का करुण समर, अभिमन्यु की वीरगति, और जयद्रथ का वध हर प्रसंग नायकत्व की जटिलता और धर्म अधर्म की परतें खोलता है ! युद्ध के बाद अधिकांश महारथी नहीं बचते ! युधिष्ठिर राजसिंहासन पर बैठते हैं पर विजय में शोक का धुआँ घुला रहता है ! शांति और अनुशासन पर्व में भीष्म शरशय्या पर पड़े पड़े राजधर्म, आपद्धर्म और जीवन नीति का पाठ देते हैं और अंत में पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर मोक्ष की तलाश करते हैं !
प्रमुख पात्र
- कृष्ण : सखा और सारथी ! कठिन क्षणों में नीति और व्यवहार का संतुलन दिखाते हैं ! उनका उपदेश कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम है !
- अर्जुन : सिद्धहस्त धनुर्धर पर भीतर से संशयग्रस्त ! उनकी दुविधा कई बार हमारी अपनी नैतिक उलझन लगती है !
- युधिष्ठिर : सत्य निष्ठ राजा ! पर नीति और व्यावहारिकता के बीच कई बार फँस जाते हैं ! द्यूत सभा का उनका मौन आज भी खटकता है !
- भीम : बल और संकल्प के प्रतीक ! अन्याय के प्रतिकार की साफ़ आवाज़ !
- द्रौपदी : साहस और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति ! न्याय की आवाज़ बनकर सत्ता के ढोंग को चुनौती देती हैं ! यह प्रसंग दिल को हिला देता है !
- कर्ण : दानवीर और अद्वितीय धनुर्धर ! त्रासदी जन्म गोपन और निष्ठा के टकराव में ! आत्म सम्मान बड़ा पर मित्रता की कीमत भी भारी !
- भीष्म : प्रतिज्ञा निष्ठ, नीति परायण, परंपरा के बोझ से विवश ! आदर्श और यथार्थ के बीच फँसा व्यक्तित्व !
- दुर्योधन : अधिकार बोध से प्रेरित शासक ! मैत्री ( कर्ण ) और द्वेष ( पांडव ) के बीच जिद्दी खड़ा !
- शकुनि : द्यूत और षड्यंत्र का केंद्र ! सत्ता के अनैतिक साधनों की कीमत दिखाता है !
- द्रोण और कृप : आचार्यत्व, शौर्य और शिष्य निष्ठा की उलझन भरी छवियाँ !
- विदुर : स्पष्टवक्ता नीति परामर्शदाता ! सत्ता के सामने भी विवेक नहीं छोड़ते !
महाभारत का हृदय उसके दार्शनिक संवाद में धड़कता है ! भगवद्गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति तीनों रास्तों से अर्जुन के मोह का निवारण किया जाता है ! मूल प्रश्न यह नहीं कि युद्ध उचित है या नहीं ! प्रश्न यह है कि जब सारे विकल्प चुक जाएँ तब कर्तव्य क्या है ! यही धर्म है परिभाषा नहीं, संदर्भ संवेदनशील विवेक !
यहाँ सत्य की रेखाएँ साफ़ नहीं होतीं ! भीष्म धर्म के आग्रह में निर्णायक हस्तक्षेप टालते हैं ! युधिष्ठिर सत्यवादी हैं फिर भी द्यूत सभा में मौन रहकर अपराध के हिस्सेदार बनते हैं ! कर्ण उदार हैं, पर अन्यायपूर्ण परियोजना के साथ खड़े दिखाई देते हैं ! और यहीं से, ग्रंथ उपदेश से आगे जाकर अनुभव का रूप लेता है ! मानो घर का कोई अपना सवाल कर रहा हो तुम क्या करते ?
…
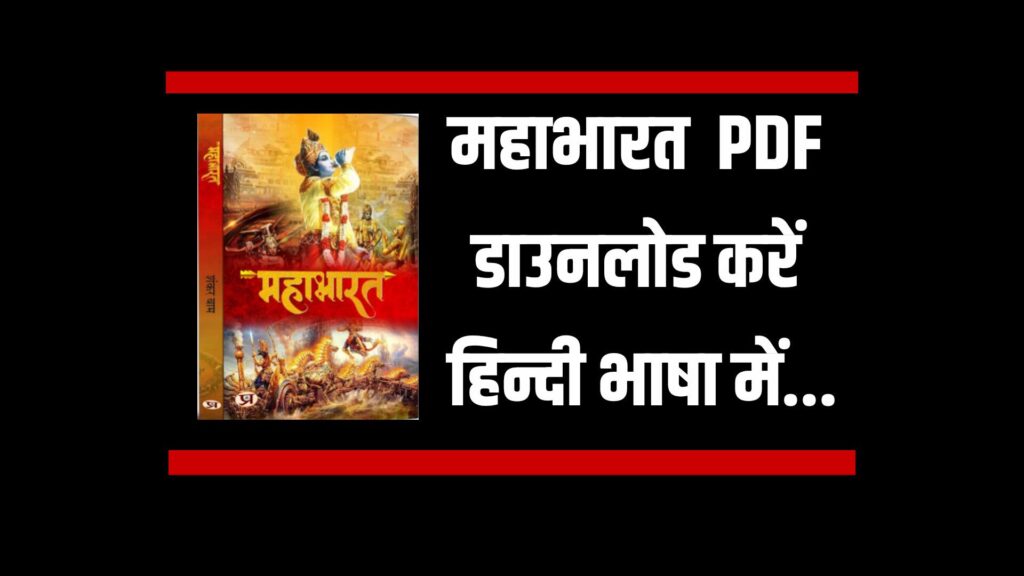
…
प्रमुख प्रसंग
- द्यूत सभा और द्रौपदी का प्रश्न : ” सभा क्या है ? धर्म क्या है ? ” शक्ति के सामने नैतिकता की असहायता और फिर उसके पुनर्स्थापन की जद्दोजहद !
- लक्षागृह : सत्ता संघर्ष में छल का शुरुआती बिगुल !
- विराट पर्याय ( अज्ञातवास ) : आत्मसंयम और रणनीतिक धैर्य का समय ! अर्जुन का बृहन्नला वेश पाठकों को चौंकाता भी है और सिखाता भी !
- गीता उपदेश : युद्धभूमि पर जीवन नीति का पाठ कर्म, समत्व और समर्पण का संवाद !
- अभिमन्यु की वीरगति : साहस का दुखांत पक्ष ! यह प्रसंग पढ़ते हुए गरदन झुक जाती है !
- जयद्रथ वध : समय नीति और युद्धकौशल का बेजोड़ समन्वय !
- भीष्म की शरशय्या : शांति और अनुशासन पर्व का ज्ञान भंडार राज्य, समाज और नैतिकता पर विस्तृत विमर्श !
राजधर्म केवल शांति रक्षा नहीं, न्याय की स्थापना है ! सीधी बात तो यही है : जब संस्थाएँ सभा, गुरु, कुल नैतिक साहस खो देती हैं तो अन्याय बढ़ता है और युद्ध अनिवार्य हो जाता है ! द्रौपदी, कुंती, गांधारी इनके अनुभव समाज में स्त्री स्वर के उदय और उसकी अनसुनी पीड़ा दोनों को सामने लाते हैं !
…
…
…
आर्थिक सामाजिक परतें भी उतनी ही तेज हैं द्यूत, कर व्यवस्था, दान धर्म, वरदान श्राप, शिक्षा और शस्त्र एकाधिकार ! कर्ण का चरित्र वंश, उत्पत्ति और अवसर समानता का कठिन सवाल उठाता है ! आज के प्रशासन में भी कभी कभी कोई निर्णय तात्कालिक राहत देता है पर जब जन विश्वास नहीं बनता तो वही निर्णय अगले मोड़ पर भारी पड़ता है ! यही सबसे बड़ा सबक है : राज्य तभी टिकता है जब नैतिक वैधता और जन सम्मति साथ हों नहीं तो विजय भी क्षय में बदल जाती है !
महाभारत की भाषा कथा प्रधान है पर उसमें संवाद, उपाख्यान, दृष्टांत और नीति सूक्तियाँ भी बहती रहती हैं ! एक कथा के भीतर दूसरी कथा, ऋषि मुनियों के प्रसंग, तीर्थयात्राएँ, दान, यज्ञ, लोक जीवन ! इस बहुलता से अर्थ स्तर खुलते जाते हैं ! वीर रस है, करुण रस है, और शांति रस का विस्तार भी ! पाठक केवल दर्शक नहीं रहता, सहभागी बन जाता है !
कभी कभी लगता है यह ग्रंथ हमें सांस लेने की लय सिखाता है धीरे, फिर तेज, फिर ठहराव ! जैसे जीवन !
महाभारत हमारी स्मृति, भाषा और कला में गहरे उतर चुका है ! शास्त्रीय और लोक नाट्य में इसकी मजबूत उपस्थिति है ! यक्षगान और कथकली में द्रौपदी वस्त्रहरण और भीष्म शरशय्या के प्रसंग विशेष लोकप्रिय हैं ! पेंटिंग, मूर्तिकला, नृत्य नाट्य, टीवी और फिल्मों में इसके रूपांतरण मिलते हैं ! बोलचाल में मुहावरे आज भी जीवित हैं ” चौपड़ का खेल “, ” भीष्मप्रतिज्ञा “, ” कर्ण दान “, ” द्रोणाचार्य शिष्य ” !
यह सब देखकर कई बार मन कहता है यह केवल किताब नहीं, एक जीती जागती परंपरा है !
आधुनिक काल में पुनर्पाठ अनेक दिशाओं में हुआ है ! बी.आर. चोपड़ा की टीवी श्रृंखला में द्रौपदी वस्त्रहरण का दृश्य प्रसारित हुआ तो कई घरों में सन्नाटा छा गया ! मैंने खुद अपने पड़ोस में देखा, लोग टीवी के सामने खड़े हो गए थे, जैसे दरबार में अन्याय उनके सामने हो रहा हो ! बिबेक देब्राय के अंग्रेजी अनुवाद ने सरल भाषा में जटिल अर्थों को बचाए रखा है, जिससे नए पाठकों के लिए दार्शनिक परतें खुलती हैं !
स्त्रीवादी दृष्टि द्रौपदी, कुंती और गांधारी के अनुभवों से लैंगिक न्याय पर तीखे सवाल उठाती है ! अस्तित्ववादी और मनोवैज्ञानिक पढ़त अर्जुन की दुविधा, युधिष्ठिर के अपराध बोध और कर्ण की अस्मिता के संकट को केंद्र में रखती है ! राजनीतिक विज्ञान में इसे वैधता, प्रभुत्व, युद्ध नीति और संस्थागत पतन के अध्ययन के रूप में पढ़ा गया है ! और हाँ, प्रबंधन की कक्षा में भी यह आता है कृष्ण की सलाह, युधिष्ठिर का नैतिक कम्पास, भीष्म की प्रतिज्ञा का लागत लाभ, दुर्योधन कर्ण की टीम गतिशीलता !
अब कठिन हिस्से की बात ! भीष्म पर मतभेद हैं : एक पठन उन्हें आदर्श मानता है, दूसरा कहता है कि उनके मौन और वचन बंधन ने अन्याय को बढ़ने दिया ! युधिष्ठिर के मौन पर भी दो दृष्टियाँ टकराती हैं राजधर्म तर्क बनाम नैतिक पलायन का आरोप ! कर्ण पर तो और भी : वे दानवीर हैं, पर गलत पक्ष में खड़े ; निष्ठावान हैं, पर निजी अपमान और अस्मिता के बोझ से झुके हुए !
कृष्ण की नीति पर भी प्रश्न उठाया गया है क्या न्याय साधन के लिए छल युक्त उपाय उचित हैं और क्या यह मॉडल अहिंसक संदर्भों में भी वैध ठहरता है ? क्या यह निष्कर्ष सुविधाजनक है ? शायद नहीं ! लेकिन प्रश्न बने रहना ही इस ग्रंथ की शक्ति है ! सच कहूँ तो, यहीं महाभारत सबसे मानवीय लगता है यह हमें सोचते रहने पर मजबूर करता है !
आज जब सूचना की बाढ़, निर्णय का दबाव और नैतिक अस्पष्टता साथ चल रहे हैं, महाभारत मार्गदर्शन देता है ! साधन और साध्य, दोनों की जाँच जरूरी है ! मित्रता, निष्ठा और कर्तव्य का अर्थ संदर्भ पर निर्भर है ! और मौन भी सहभागिता हो सकता है ! नीति-निर्णयों में अक्सर तात्कालिक राहत बनाम दीर्घकालिक वैधता का टकराव दिखता है ; यही जगह है जहाँ यह ग्रंथ हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है !
कभी कभी मैं गीता का कोई श्लोक पढ़ता हूँ और ठिठक जाता हूँ क्या मैं अपने स्वधर्म को पहचान पा रहा हूँ या सुविधा के आगे झुक रहा हूँ ?
महाभारत एक समग्र मनुष्य चित्र है, पर इससे भी बढ़कर, यह हमारे भीतर उठते छोटे छोटे सवालों की गूंज है ! वीरता है ! करुणा है ! छल है ! और एक स्थायी दुविधा भी है ! धर्म कोई स्थिर सूत्र नहीं बल्कि बदलते संदर्भों में जागा हुआ विवेक है ! इसलिए यह ग्रंथ आज भी हमें पढ़ता रहता है !
सीधी बात तो यही है : शक्ति का मूल्य तभी है जब वह न्याय से जुड़ी हो ! जीत की कीमत विवेक है ! और आख़िर में एक उल्टा सवाल छोड़ दूँ कृष्ण की युद्ध नीति जिसने अन्याय के विरुद्ध न्याय का रास्ता बनाया, क्या वही नीति शांति के समय संस्थागत सुधारों में भी उतनी ही नैतिक है ? यहीं से संवाद शुरू होता है, खत्म नहीं !

