Ramcharitmanas PDF Download in Hindi | रामचरितमानस की E Book डाउनलोड करें हिंदी भाषा में
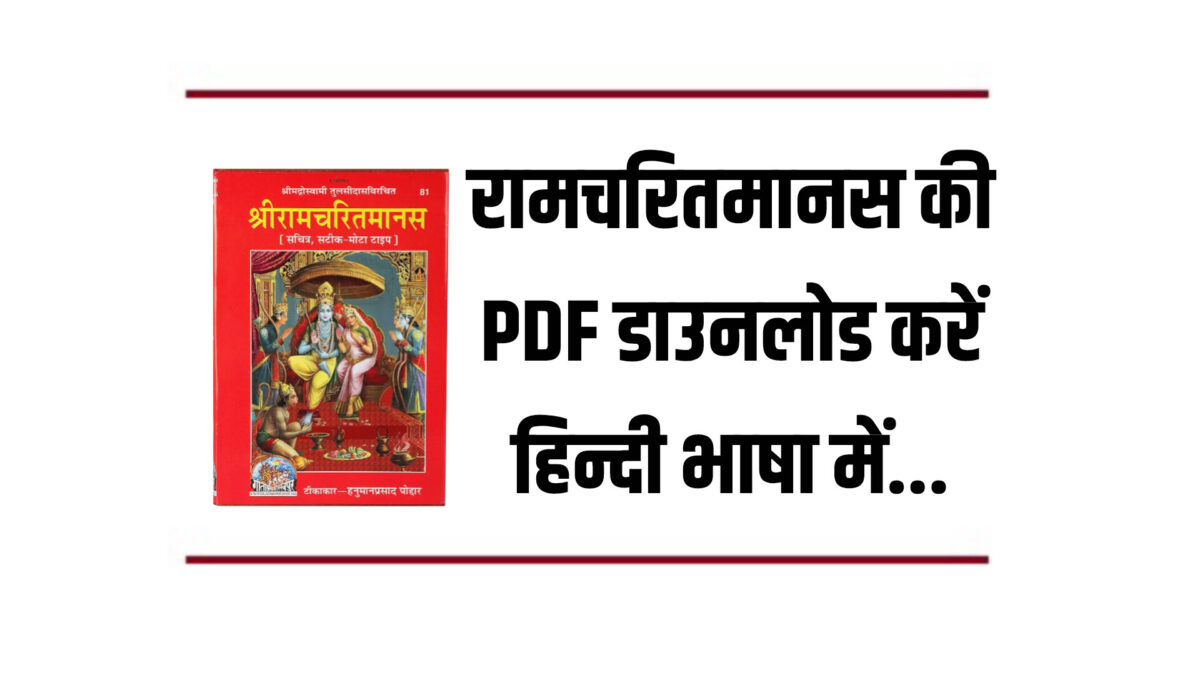
रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, कई घरों की साँसों में घुली हुई कथा है ! पहली बार मैंने इसे गाँव के चौपाल में सुना था लाउडस्पीकर खड़खड़ाता था, पर चौपाइयों की लय सीधी दिल तक उतर जाती थी ! क्या यह अचरज की बात नहीं कि चार सदी पहले लिखी गई यह कथा आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है ? ऐसा क्यों है कि जब कोई ” श्रीरामचरितमानस ” का पाठ छेड़ता है तो माहौल अपने आप नम्र हो जाता है, जैसे हवा भी धीमे धीमे सुनने लगती हो ?
जब मैंने पहली बार सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ा, लगा हनुमान मेरे भीतर साहस भर रहे हैं जैसे कोई कंधे पर हाथ रखकर कहे, ” चलो, डर है तो क्या हुआ, कोशिश तो करो ! ” उस दिन समझ आया कि मानस सूचना नहीं, संगत है ! व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ती ! आप थकें तो यह आपके लिए आसन बिछा देती है ; आप बिखरें तो यह आपको समेटती है ! क्या यही वजह नहीं कि घर घर में अखंड पाठ, कीर्तन, रामलीला अब भी धूमधाम से होते हैं ?
चार बातें, जो हर बार मानस को नया बना देती हैं !
- यह हमारी भाषा में है अवधी की मिठास, लोक उक्तियाँ, घर के आँगन की खुशबू !
- यह कथा होते होते नीति बनती है कोई उपदेश ऊपर से नहीं, सब कहानी में घुला !
- इसमें करुणा की धारा है केवट, शबरी, निषाद, हर छोटा बड़ा पात्र सम्मान के साथ उपस्थित !
- और सबसे बढ़कर, इसमें नाम स्मरण की ऐसी सहज राह है कि कठिन समय में जी संभल जाए !
कभी सोचा है, धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी इसमें कितनी रोज़मर्रा की बातों का ख्याल है वचन पालन, शरणागत की रक्षा, सेवा, संयम ? यही तो जीवन है !
बालकांड पढ़ते हुए मुझे हर बार बचपन के त्योहार याद आते हैं घर में कागज़ की पताकाएँ, गुड़ की खुशबू, और दादी की आवाज़ : ” सुनो, अब सीता स्वयंवर आया ! ” अयोध्याकांड आते ही माहौल बदलता है मन जरा भारी, पर भीतर कहीं यह भरोसा कि सही राह कठिन हो सकती है, पर बेकार नहीं जाती ! अरण्यकांड में ऋषियों के आश्रम, सूने वन, शबरी की कुटिया सब कुछ इतना जवाँ लगता है कि मानो कैमरा आँख बनकर पीछे पीछे चल रहा हो ! किष्किंधाकांड में दोस्ती की आँच है सुग्रीव का संकोच, बाली का वर्चस्व, और राम का सधी हुई नीति ! सुंदरकांड ? यह तो मानो मन का दौड़ना है लाँघ लाँघकर बाधाएँ पार ! लंकाकांड में युद्ध है, पर साथ ही धर्म का संतुलन ! और उत्तरकांड यह आसान नहीं ! यही जीवन के सबसे मुश्किल प्रश्न पूछता है : शासन और संवेदना का तालमेल कैसे बनता है ?
क्या यह अद्भुत नहीं कि हर कांड हमारे भीतर किसी न किसी अनुभव को छूता है बालपन की चमक, युवा संघर्ष, जिम्मेदारी का भार, सेवा का भाव, और अंत में दूरदर्शी विवेक ?
लोक संदर्भ : छोटी छोटी झलकियाँ
- रामलीला की एक रात मुझे याद है ! रामनगर की गलियों में भीड़, मिट्टी की सोंधी महक, और मंच पर विभीषण का शरणागति संवाद ! पास बैठे एक बुजुर्ग फुसफुसाए, ” बेटा, शरण में आए को कभी खाली मत भेजना ! ” मानो पूरी शिक्षाशास्त्र एक पंक्ति में समा गया !
- गाँव में भजन कीर्तन के दौरान जब कोई ” बिनु हरि कृपा मिलइ नहिं संता ” गाता, मेरी चाची आँखें बंद कर लेतीं उनके चेहरे पर भरोसे की ऐसी चमक कि लगता था, दुनिया की चिंता उतर रही हो !
- एक बार केवट प्रसंग पर मेरे शिक्षक ने हँसते हुए कहा, ” सेवा का मूल्य पैसा नहीं, स्पर्श है ! ” तब समझ आया, तुलसीदास ‘ सम्मान ‘ को किस महीन धागे से जोड़ते हैं !
अवधी का रस यही है कि बड़े से बड़ा भाव भी घर सा लगता है ! दोहा चौपाई की चाल कहीं धीमी, कहीं तेज जैसे कोई दादी कहानी सुनाते सुनाते रुक जाए, ” अरे, ध्यान से सुनो ! ” और फिर आगे बढ़े ! क्या आपने ध्यान दिया है चौपाई स्थिरता देती है, दोहा फैसला सुनाता है ! इसी लय के कारण मानस पढ़ना नहीं, सुनना अच्छा लगता है ! और बोलचाल की झलक चौपाल, परछत्ती, घाट, अखाड़ा सब शब्द मानो ब्रश स्ट्रोक्स हों !
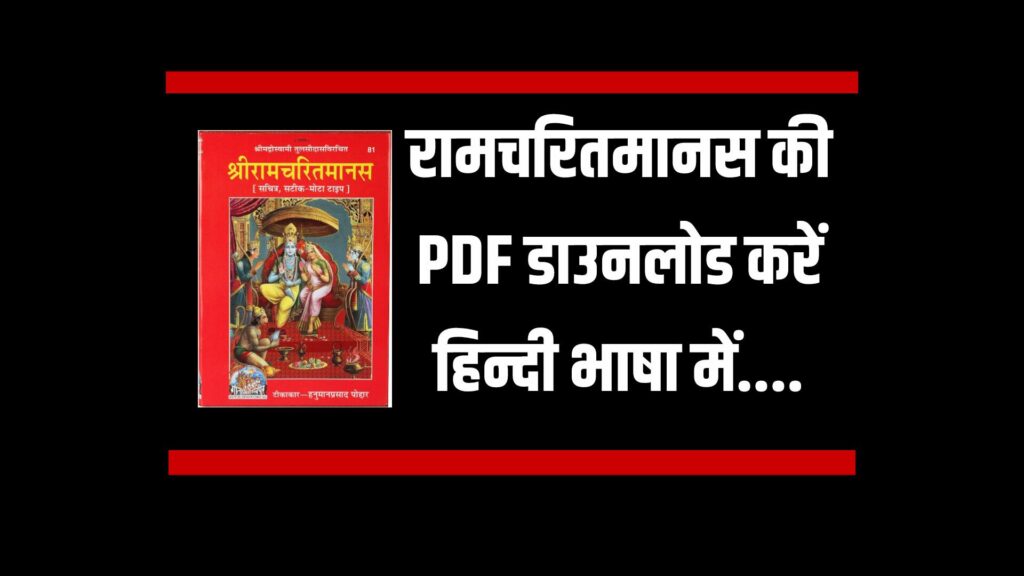
मैंने एक बार शहर के एक पाठ में देखा, मंच पर कोई भारी भरकम व्यक्तित्व नहीं था ! चार साधारण लोग, हारमोनियम, ढोलक, और एक साधु की मुस्कान ! फिर भी माहौल में ऐसा संचार कि हर पंक्ति पर ” वाह ” निकलती ! भाषा की यही ताकत है जहाँ विद्वता भी घुटने टेक दे !
सुंदरकांड पढ़ते हुए एक वाक्य बार बार भीतर गूँजता है ” रामकाज कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम ! ” क्या सेवा इतनी सहज भी हो सकती है कि अपने सुख दुख पीछे रह जाएँ ? मुझे याद है, कठिन दिनों में मैंने इसी पंक्ति को सहारा बनाया ! छोटे छोटे काम किसी की फाइल आगे बढ़वा देना, किसी मित्र के लिए समय निकालना और सच मानिए, चिंता कम हुई ! हनुमान सिखाते हैं, शक्ति का शोर मत करो ; उसे काम में लगाओ ! और यह भी कि विनय के बिना पराक्रम अधूरा है !
आज जब हम स्त्री पात्रों पर नए सिरे से सोचते हैं, तो सीता का धैर्य हमें नए सवालों के सामने खड़ा करता है ! उनकी अग्नि परीक्षा इस पर मन भारी भी होता है और जिज्ञासा भी ! उस समय के लोकधर्म, राजधर्म, और निजी गरिमा का टकराव यह सब सरल नहीं ! क्या करुणा का शासन हमेशा सही निर्णय देता है ? क्या आदर्श कभी कभी व्यक्ति पर कठोर हो जाता है ? मुझे लगता है, इन प्रश्नों को ठुकराना नहीं चाहिए ! सीता की शांत गरिमा अशोक वाटिका की निर्भीकता, रामराज्य में उनकी आत्म स्थापना ये सब हमें बताती हैं कि मौन भी प्रतिरोध हो सकता है ! आलोचना यहाँ संवेदना के साथ हो ताकि हम उस युग को समझते हुए अपने समय के लिए न्याय और सम्मान की राह निकाल सकें !
.
.
राम का चरित्र जितना बड़ा, उतना ही सधा हुआ ! वे चमत्कारों के नायक नहीं, चयन के नायक हैं ! वनवास कितना सरल था ” ना ” कहना, पर उन्होंने ” हाँ ” कहा, क्योंकि वचन उनके लिए शक्ति से बड़ा था ! विभीषण शरणागति में उनका निर्णय ” जो शरण आए, वह अपना ” आज की भाषा में कहें तो यह सिद्धांत आधारित नेतृत्व है ! और रावण ? उसकी विद्वता पर अहंकार का पर्दा ! यह हमें चेताती है ज्ञान बिना विनम्रता, तलवार बिना मयान !
कभी कभी लगता है, राम उसी धीमी लौ जैसे हैं जो आँधी में भी टिमटिमाती रहती है ! तेज़ नहीं, पर भरोसेमंद !
रामराज्य सिर्फ किताबों की बात नहीं, यह आज भी लोगों के मन का सपना है ! एक ऐसा समाज जहाँ न्याय कठोर नहीं, संवेदनशील हो ; जहाँ शासन पारदर्शी हो ; जहाँ कमजोर को पहले याद किया जाए ! पंचायत से लेकर संसद तक क्या हम यह पूछ सकते हैं कि हमारे निर्णयों में करुणा की कितनी जगह है ? मुझे याद है, एक जिलाधिकारी ने कहा था, ” फाइल पर सिग्नेचर तब करता हूँ जब समझ जाता हूँ कि इस कागज के पीछे किसी की रसोई, किसी बच्चे की फीस जुड़ी है ! ” यही तो रामराज्य की सोच है नियम, पर मानवीय संवेदना के साथ !
किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ पर विमर्श ज़रूरी है ! मानस की कुछ चौपाइयों पर आज सवाल उठते हैं स्त्री दृष्टि, जाति संदर्भ, दंड की कठोरता ! इन पर चर्चा होनी चाहिए ! लेकिन क्या यह उचित नहीं कि हम पाठ परंपरा, ऐतिहासिक संदर्भ और लेखक के अभिप्राय को साथ रखकर पढ़ें ? तुलसीदास का मूल स्वर समन्वय का है जहाँ शबरी की जूठी बेर भक्ति की सबसे ऊँची परिभाषा बन जाते हैं, और केवट की सेवा राजसी आडंबर से बड़ी हो जाती है ! तो क्या हमारा रास्ता ‘ रद्द ‘ करने का है या ‘ पुनर्पाठ ‘ का ? मेरी विनती है हम प्रश्न पूछें, पर करुणा की नज़र से ! ताकि ग्रंथ की आत्मा सम्मान, शरण, सेवा हमारे समय की समानता और गरिमा के स्वर में घुल जाए !
मानस पढ़ने से ज़्यादा गाने में खुलता है ! चौपाइयों की लय, आलाप का उठना बैठना, ढोलक का धीमा थपका यह सब मिलकर कथा को देह देते हैं ! एक बार रामनवमी की रात मैंने देखा, मंच पर कलाकार नहीं पहुँचे ! तब गाँव के युवक ही बन गए राम लक्ष्मण ! उनकी आवाज़ काँप रही थी, पर दर्शक मंत्रमुग्ध ! मुझे लगा, यही तो मानस का चमत्कार है यह मंच का नहीं, मन का नाटक है !
आज के लिए कुछ सरल सूत्र
- वचन पालन : रिश्तों की नींव !
- शरणागत की रक्षा : सत्ता हो या साधारण जीवन जो मदद माँगे, उसे निराश न करें !
- सेवा भक्ति : काम में भक्ति का भाव बिना शोर, बिना अपेक्षा !
- संतुलन : नीति में संवेदना, और संवेदना में विवेक !
- पुनर्पाठ : परंपरा को प्रेम से, पर आँखें खोलकर पढ़ना !
क्या यह सब किसी कॉर्पोरेट मीटिंग, किसी स्कूल असेंबली, किसी परिवार की साप्ताहिक बैठक में काम नहीं आ सकता ? बिल्कुल !
तुलसीदास अध्यात्म को पहाड़ की चोटी से उतारकर रसोई के धुएँ में मिला देते हैं ! ” बन्दउँ गुरु पद कंज… ” से शुरू होती विनय, कब केवट के नाव भाड़े में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता ! यही उनकी कला है ऊँचे विचार, पर पाँव मिट्टी में ! वे हमें बताते हैं : आदर्श दूर का तारा नहीं ; यह छोटी छोटी ईमानदारियों से बनता है समय पर पहुँचना, झूठ न बोलना, लालच से बचना, और जहाँ बन पड़े, किसी का भार हल्का कर देना !
मैंने कई बार देखा, कठिन दिन में भी जब किसी ने ” सीताराम ” कहा, चेहरे पर ढील पड़ गई ! जैसे भीतर की गाँठ थोड़ी खुल गई हो ! शायद यही मानस का सबसे बड़ा वरदान है यह हमें कठोर नहीं, कोमल बनाती है ; पर उस कोमलता में हिम्मत है !
रामचरितमानस भारत की सामूहिक स्मृति का वह दीप है जो मंदिर की देहरी से ज़्यादा घर की चौखट पर जलता है ! यह ग्रंथ बताता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, रोज़मर्रा का न्याय है ; भक्ति केवल आँसू नहीं, जिम्मेदारी भी है ; और राम वे केवल पूज्य नहीं, अनुकरणीय हैं ! हम जब जब इस कथा को अपनाते हैं, अपने भीतर की शक्ल कुछ साफ़ होती है ! क्या यही ” मर्यादा ” की असली परिभाषा नहीं शक्ति को अनुशासन देना, और प्रेम को व्यवहार ?
मेरी अनुभूति यही कहती है : मानस पढ़ना एक यात्रा है बचपन से युवावस्था, व्यक्तिगत से सामाजिक, और अंततः भय से भरोसे तक ! इस राह पर जो भी कदम बढ़ाता है, उसे कहीं न कहीं अपना एक छोटा सा अयोध्या मिल ही जाता है मन के भीतर !

