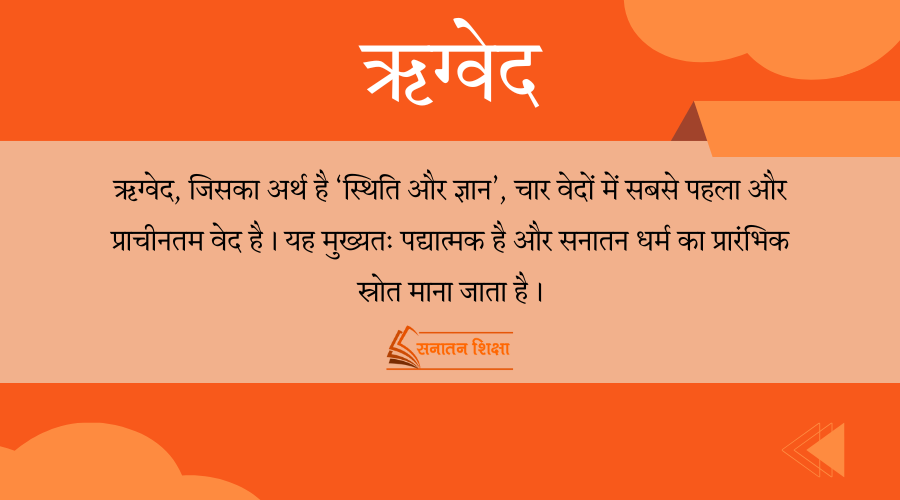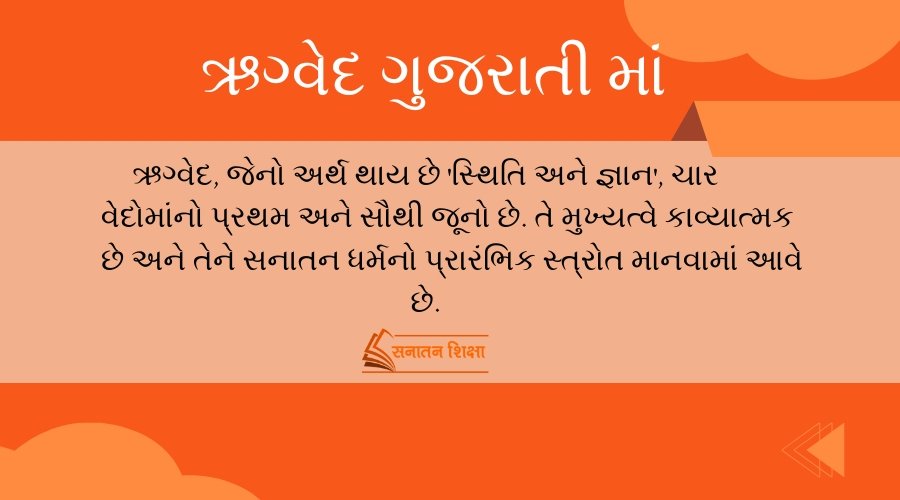श्रीमद्भागवत गीता तीसरा अध्याय संपूर्ण सार हिंदी भाषा में :-
श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय का नाम “कर्मयोग” है। यह अध्याय कर्म (कर्तव्य) और उसके महत्व पर केंद्रित है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। इस अध्याय का सार यह है कि कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति आत्म-शुद्धि और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है।
आइए इसे विस्तार से समझें:-
मुख्य बिंदु:
कर्म का अनिवार्य स्वरूप:-
श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। प्रकृति के गुणों (सत्त्व, रजस, तमस) के प्रभाव के कारण हर प्राणी को कर्म करना पड़ता है। यहाँ तक कि जीवन को बनाए रखने के लिए भी कर्म आवश्यक है। इसलिए कर्म को त्यागना संभव नहीं है।
निष्काम कर्म का महत्व:-
कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है और स्वार्थ या आसक्ति से दूर रहता है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह निष्काम कर्म ही कर्मयोग का आधार है।
अर्जुन का संशय और समाधान:-
अर्जुन पूछते है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो उसे युद्ध जैसे हिंसक कार्य में क्यों लगाया जाए। श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म एक-दूसरे के पूरक हैं। कर्म त्यागने से नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से करने से ज्ञान प्राप्त होता है। युद्ध अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है, और उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए।
लोकसंग्रह (समाज के लिए उदाहरण):-
श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं कर्म करते हैं, हालाँकि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसका कारण यह है कि यदि श्रेष्ठ लोग कर्म छोड़ दें, तो सामान्य जन उसका अनुसरण करेंगे, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोकसंग्रह (सामाजिक कल्याण) के लिए जरूरी है।
इंद्रियों का नियंत्रण:-
इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आसक्ति और कामना इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। कर्मयोगी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें वश में करके अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए।
कर्म और अकर्म की गति:-
श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म में अकर्म (निष्क्रियता) को देखना और अकर्म में कर्म को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इसका अर्थ है कि सही मायने में कर्म वह है जो आत्मा के उद्देश्य को पूरा करे, न कि केवल शारीरिक क्रिया।
प्रमुख श्लोक और उनका अर्थ:- श्लोक 3.5: “न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्…”
अर्थ: कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण सभी को कर्म करना पड़ता है।
श्लोक 3.19: “तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर…”
अर्थ: इसलिए आसक्ति छोड़कर सदा अपने कर्तव्य का पालन करो। निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है।
श्लोक 3.27: “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः…”
अर्थ: सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है।
सारांश:- तीसरा अध्याय कर्मयोग का मूल सिद्धांत स्थापित करता है: जीवन में कर्म अनिवार्य है, लेकिन उसे आसक्ति और फल की इच्छा से मुक्त होकर करना चाहिए। यह अध्याय अर्जुन को यह सिखाता है कि अपने धर्म (कर्तव्य) का पालन करना ही सच्चा मार्ग है, और इससे न केवल व्यक्तिगत शुद्धि होती है, बल्कि समाज का भी भला होता है। श्रीकृष्ण कर्म और ज्ञान के बीच संतुलन का महत्व बताते हैं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। यह अध्याय हमें जीवन में कर्तव्यनिष्ठा, निस्वार्थता और संयम का पाठ पढ़ाता है।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता की जय हो!
भगवत गीता तीसरा अध्याय सार – Geeta 3 Chapter Summary