Rigveda PDF Download in Hindi | ऋग्वेद की E Book डाउनलोड करें हिंदी भाषा में
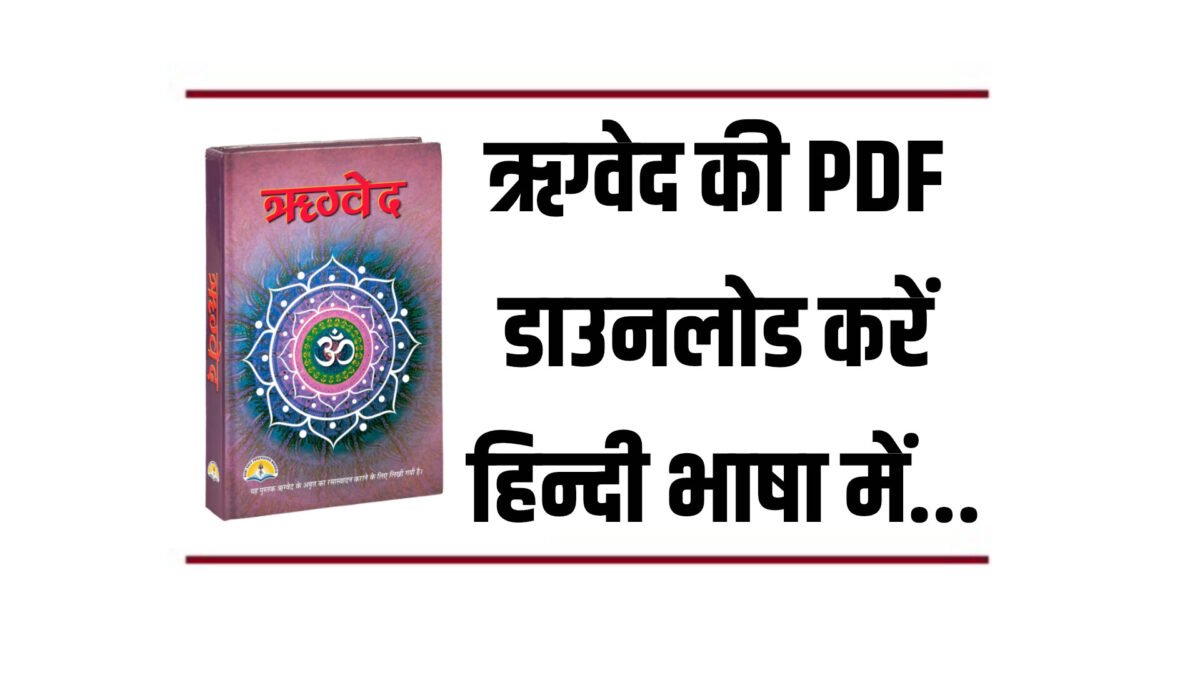
कभी कभी मुझे लगता है, ऋग्वेद का परिचय देने की कोशिश उसी तरह है जैसे सूर्योदय को शब्दों में पकड़ना कुछ न कुछ छूट ही जाता है ! यह केवल ” भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ” नहीं है ; यह एक जीवित आवाज़ है, जो प्रकृति से, मनुष्य से, और किसी अदृश्य रहस्य से बराबर बात करती है ! यहां यज्ञ स्थल की अग्नि है, तूफ़ान के मरुत हैं, भोर की उषा है और साथ ही मन में उठते बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं जो आज हम विज्ञान, दर्शन या रोज़मर्रा की उलझनों में पूछते हैं ! क्या यह संभव है कि सहस्रों साल पहले के ऋषि वही सवाल पूछ रहे थे जो आज हम पूछते हैं ?
मैं स्वीकार करता हूं ऋग्वेद को एक ही सांचे में बांधना मुश्किल है ! विद्वान इसे दस मंडलों, एक हजार से अधिक सूक्तों और लगभग दस हज़ार ऋचाओं में व्यवस्थित बताते हैं, पर पढ़ते हुए यह आंकड़े पीछे छूट जाते हैं ; सामने बस भाषा, लय और अर्थ की उठती गिरती लहरें रह जाती हैं ! सायणाचार्य ने अपने विस्तृत भाष्य में इसे यज्ञ केंद्रित अर्थव्यवस्था से जोड़ा, जबकि आधुनिक अध्ययनों जैसे माइकल वित्ज़ेल, स्टेफ़नी जैमिसन, जोएल ब्रेरटन या फ्रिट्स स्टाल ने भाषा, अनुष्ठान और इतिहास के नए कोण सुझाए ! कुछ बातों पर वे आपस में सहमत भी नहीं होते, और यही अच्छा है हल्का सा संशय लेखन को ईमानदार बनाता है !
जब मैंने पहली बार नासदीय सूक्त पढ़ा ” तब न असत् था, न सत् ” तो मन में अचानक एक शांति और बेचैनी साथ साथ आई ! शांति इसलिए कि यह सूक्त हमारे अज्ञान को स्वीकार करता है ; बेचैनी इसलिए कि अंत में यह पूछ बैठता है, ” जो सर्वोच्च है, क्या वही जानता है ?” मुझे लगा, यह किसी भी वैज्ञानिक जिज्ञासा से कम नहीं है ! हम आज भी बिग बैंग, डार्क मैटर, चेतना की उत्पत्ति पर सवाल पूछते हैं और ऋग्वैदिक ऋषि भी अपने तरीके से वही कर रहे हैं ! यह बौद्धिक विनम्रता कि शायद सबका अंतिम उत्तर अभी हमारे पास नहीं मुझे बार बार खींच लाती है !
एक और क्षण जो निजी है ! शहर की नदी के किनारे चलते हुए जहां पानी का रंग संदेह जगाता है, मुझे सरस्वती के स्तोत्र याद आते हैं जल का प्रवाह, वाणी का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह ! क्या हम सच में अपनी नदियों के साथ वैसा रिश्ता निभा रहे हैं जैसा ऋग्वेद की कल्पना है ? शायद नहीं ! और शायद यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ आज भी प्रासंगिक लगते हैं वे हमें हमारी कमज़ोरियों के आईने दिखाते हैं !
अग्नि से शुरुआत यह लगभग एक नियम सा है ! अग्नि यहां लौ भर नहीं, यज्ञ का पुरोहित है, देवताओं तक पहुंचाने वाला दूत ! इंद्र आएंगे, वज्रधारी मेघों को तोड़कर वर्षा के रास्ते खोलने वाले ! मरुतों का शोर है, उषा की रोशनी है, वरुण का नैतिक अनुशासन है, सोम की उन्नत चेतना है ! ” एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ” एक सत्य पर नाम अनेक ! क्या यह बहुलता केवल सहिष्णुता है ? मुझे लगता है इससे थोड़ा अधिक, यह विविध दृष्टियों में एक ही अनुभव की झलक पकड़ने की चेष्टा है !
भाषा वैदिक संस्कृत की है, शास्त्रीय संस्कृत से पुरानी, अधिक लचीली, ध्वनि में कहीं कहीं कच्ची सी, पर संगीत से भरी ! गायत्री, त्रिष्टुभ, जगती, छंदों की धड़कनें पढ़ते पढ़ते आप सुनने लगते हैं ! मुझे याद है पहली बार त्रिष्टुभ के चार चरणों की लय गिनते हुए लगा, यह केवल कविता नहीं यह किसी अनुष्ठान का ध्वनि स्थापत्य है ! फ्रिट्स स्टाल अक्सर वैदिक अनुष्ठानों को ” शुद्ध क्रिया संरचनाएँ ” कहते हैं ; छंदों में वह क्रियात्मक अनुशासन महसूस होता है !
कहने को ऋग्वेद की सबसे व्यवस्थित संरचनाएँ परिवार मंडलों ( द्वितीय से सप्तम ) में हैं, गृत्समद, विश्वामित्र, वसिष्ठ, अत्रि, भरद्वाज, कश्यप ! पर सच बताऊं ? पढ़ते समय यह वंशावली पृष्ठभूमि में धुंधला जाती है ! सामने बस एक जीवित आवाज़, कभी प्रार्थना, कभी स्तुति, कभी सीधे सवाल !
…
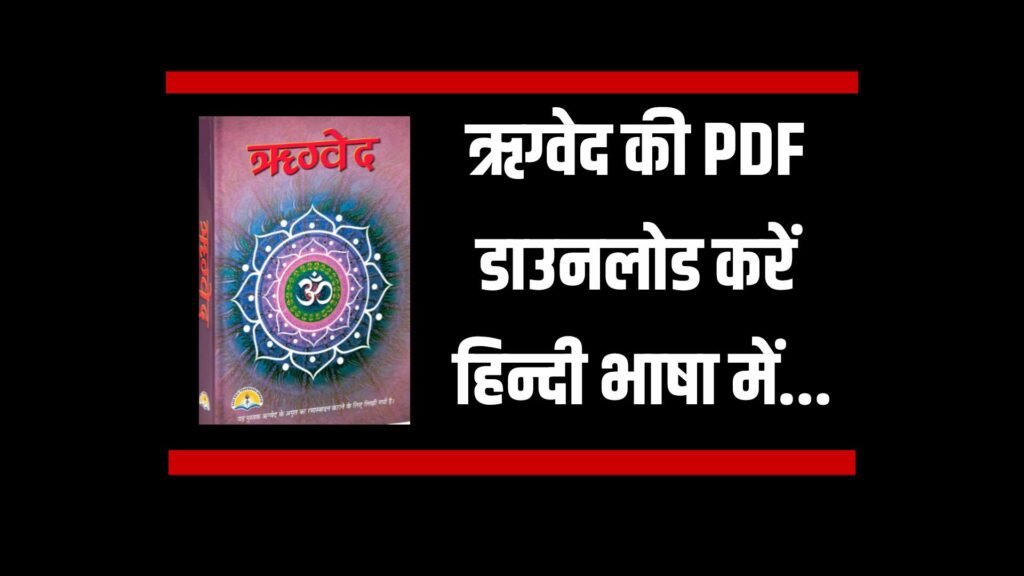
…
सभा और समिति, दो संस्थान अक्सर उल्लेख में आते हैं ! इससे लगता है कि निर्णय प्रक्रिया सामुदायिक थी, कम से कम कुछ मामलों में ! गृहस्थ जीवन का आदर्श उभरता है, दान, अतिथ्य, वचन पालन ! स्त्रियों की उपस्थिति भी साफ मिलती है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसे नाम केवल फुटनोट नहीं हैं ; वे संवाद करती हैं प्रश्न पूछती हैं ! क्या यह कथा आज के पाठक के लिए पर्याप्त है ? शायद कुछ और संदर्भ चाहिए पर इतना तो तय है कि वैदिक समाज में स्त्री की धार्मिक और बौद्धिक भागीदारी के प्रमाण हैं, भले बाद के युगों में तस्वीरें बदलती गईं !
यज्ञ का संसार, इसे केवल ” बलि आहुति ” समझना अनुचित होगा ! यहां यज्ञ भोजन साझेदारी, दान, संगीत, और एक सामूहिक धुन भी है ! अग्नि दूत है, सोम प्रेरणा ! नियम संयम, उच्चारण की सूक्ष्मता, और छंद की पवित्रता, ये सब मिलकर एक ” ध्वनि योग ” रचते हैं ! जब घनपाठ या जठापाठ की चर्चा होती है, पदों की उलट फेर के साथ पाठ की जटिल स्मृति, तो सच में हैरानी होती है कि मौखिक परंपरा ने इतने शताब्दियों तक शब्दों को कैसे बचाए रखा ! स्टेफ़नी जैमिसन और जोएल ब्रेरटन के अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ते हुए यह फर्क समझ में आता है कि उच्चारण के सूक्ष्म चिह्न अर्थ संकेतों को कैसे प्रभावित करते हैं ! और हां हर अनुवाद अधूरा होता है, यह स्वीकार करना पड़ेगा !
दर्शन की बात आए तो मुझे ऋग्वेद किसी ” सिस्टम ” जैसा नहीं लगता ! यह व्यवस्थित उपनिषद सा नहीं बल्कि प्रश्नों का उफान है ! नासदीय सूक्त का अज्ञेयवाद, पुरुष सूक्त का समष्टि पुरुष ( जिसे लेकर कुछ विद्वान सामाजिक राजनीतिक रूपक भी देखते हैं ), हिरण्यगर्भ सूक्त का सृष्टि बीज, ये सब अलग दिशाओं से एक ही क्षितिज की ओर चलते हैं ! डॉ. रोमिला थापर लिखती हैं कि वैदिक ग्रंथों को एकरेखीय और एकस्वर नहीं समझना चाहिए ; वे परतदार हैं और समय के साथ अर्थ बदलते रहते हैं ! मुझे यह बात सही लगती है, आज का पाठक शायद इनमें विज्ञान भाव, पर्यावरण चेतना, या नैतिक कन्फ्यूज़न के अपने निशान भी खोज ले !
और इतिहास ? तिथियां हमेशा विवादित रहेंगी ! सामान्य मत पंद्रह सौ – एक हज़ार ( 1500 – 1000 ) ईसा पूर्व के बीच की रचना परतों की बात करता है पर माइकल वित्ज़ेल जैसे विद्वान भाषिक और भौगोलिक संकेतों के आधार पर इससे थोड़ी सूक्ष्म आंतरिक डेटिंग सुझाते हैं ! कुछ भारतीय विद्वान इससे असहमत भी हैं ! मैं यहां कोई अंतिम ध्वज नहीं गाड़ना चाहता, इतिहास की जमीन पर संदेह का एक पत्थर रहना चाहिए तभी बहस जीवित रहती है !
तीन बातें मुझे आज के संदर्भ में बार बार लौटाती हैं ! पहली, प्रकृति का संबंध ! नदियों के स्तोत्र, उषा की सूक्तियां, वरुण का ऋत, यह सब बताता है कि प्राकृतिक और नैतिक नियमों को अलग अलग खांचे में रखकर नहीं देखा गया था ! आज जब हम पर्यावरण नीति पर बात करते हैं तो क्या यह दृष्टि, प्रकृति नियम और नैतिक नियम का साझा संतुलन, कुछ प्रेरणा देती है ? शायद हां, कम से कम एक संवेदनशीलता तो देती ही है !
दूसरी, बहुलता ! ” एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ” केवल एक पंक्ति नहीं एक अभ्यास है ! अलग देवता, अलग प्रतिमान, अलग नाम, पर किसी एक गहरे अनुभव की टटोल ! बहुसांस्कृतिक समाजों में यह रुख, कि अलग होकर भी साथ रहना संभव है, कम महत्वपूर्ण नहीं ! यह कोई आसान काम नहीं पर वैदिक कल्पना इसे स्वाभाविक मानती है !
तीसरी, जिज्ञासा और विनम्रता ! वह आखिरी सवाल, ” क्या निर्माता स्वयं जानता है ? “, मुझे बार बार याद दिलाता है कि ज्ञान का पहला कदम स्वीकार करना है कि हम सब नहीं जानते ! यह वैज्ञानिक पद्धति का भी एक मूल भाव है ! ए.एल. बाशम ने भारतीय परंपराओं की ” वंडरिंग माइंड ” की बात कही है, मुझे नासदीय सूक्त में वही मन घूमता दिखता है !
यही वजह है कि ऋग्वेद की चर्चा केवल पूजा पाठ की बहस नहीं है ! यह शिक्षा, सार्वजनिक नीति, और यहां तक कि व्यक्तिगत नैतिकता में भी धीरे धीरे रिसती हुई एक आवाज़ है, कभी धीमी, कभी तीखी !
शाकल संहिता आज मानक पाठ है ; बाष्कल परंपरा का उल्लेख मिलता है पर वह कम उपलब्ध है ! पदपाठ, क्रमपाठ, जठापाठ, घनपाठ, यह सब केवल शास्त्रीय कौशल नहीं एक सांस्कृतिक स्मृति तकनीक है ! राल्फ़ ग्रिफ़िथ जैसे पुराने अनुवादक हों या जैमिसन ब्रेरटन जैसे आधुनिक विद्वान, सभी इस मौखिक विरासत के आगे विनम्र दिखते हैं ! सायणाचार्य के भाष्य से लेकर निरुक्त परंपरा तक और आधुनिक तुलनात्मक मीमांसा तक व्याख्या का वृक्ष बहुत घना है ! कुछ फल मीठे हैं, कुछ कड़वे, और कुछ शायद अभी कच्चे !
प्रभाव ? सूची लंबी हो जाएगी ! उपनिषदों की दर्शन धारा, गीता की आत्म संवाद शैली, भक्ति काव्य का सरगम, शास्त्रीय संगीत की स्तोत्र गायन परंपरा, सब कहीं न कहीं ऋग्वैदिक बीजों से निकले ! कभी कभी लगता है हमारी भाषाओं की बुनियाद में भी ऋग्वेद की ध्वनियां गूंजती हैं, शायद यह अतिशयोक्ति हो पर यह एहसास बुरा नहीं !
और हां, प्रतिपक्ष भी ज़रूरी है ! कुछ विद्वान मानते हैं कि हम ऋग्वेद में ” आधुनिक ” अर्थों की ज्यादा तलाश कर लेते हैं, पर्यावरणवाद, नारीवाद, विज्ञान, जो उसके अपने संदर्भ का हिस्सा नहीं थे ! यह चेतावनी ठीक है ! पर क्या किसी क्लासिक ग्रंथ का सौंदर्य यही नहीं कि वह नए संदर्भों में नए अर्थ उगाता है ? मैं यहां दोनों और का पक्ष लेता हूं, मूल संदर्भ का सम्मान और नए अर्थों की अनुमति, दोनों साथ !
अंत में, मैं कोई अंतिम विधान नहीं देना चाहता ! ऋग्वेद को एक सख्त खांचे में बंद करने से उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है ! बेहतर है कि हम उसे पढ़ें, कभी छंद की लय में, कभी देवताओं की कहानियों में, कभी नासदीय जैसे सूक्तों की चुप्पी में ! मुझे लगता है यही ग्रंथ हमें सिखाता है, बहुलता में एक धागा, जिज्ञासा में विनम्रता, और शक्ति में मर्यादा ढूंढ़ना ! और अगर आप मुझसे पूछें कि ऋग्वेद आज क्यों पढ़ना चाहिए तो मेरा सीधा जवाब होगा : ताकि हम अपने सवालों से थोड़ा और ईमानदारी से मिल सकें, और शायद कभी कभी उनसे दोस्ती भी कर लें !

